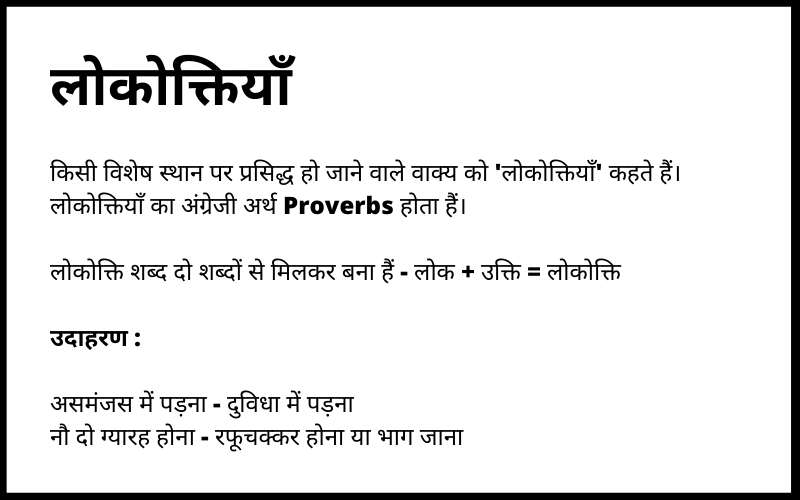दैनिक जीवन में लोकोक्तियाँ का उपयोग करके भाषा शैली को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी लोकोक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पेज पर हमने हिंदी लोकोक्तियाँ जानकारी शेयर की है।
पिछली पोस्ट में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अध्याय हिंदी मुहावरे की जानकारी शेयर की है वह जरूर पढ़े।
तो चलिए इस पेज पर लोकोक्तियाँ की सामान्य जानकारी से पढ़ना शुरू करते है।
लोकोक्तियाँ किसे कहते है
किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ‘लोकोक्ति’ कहते हैं।
दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते है।
लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैं – लोक + उक्ति = लोकोक्ति
अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती हैं लोकोक्ति कहलाती हैं। लोकोक्तियों को कहावत, सुक्ति आदि नामों से जाना जाता हैं।
उदाहरण :- एक दिन बात ही बात में श्याम ने कहा “हाँ” मैं अकेला ही कुँआ खोद लूँगा।
इस बात पर एक व्यक्ति ने हँसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।
यहाँ ‘अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता’ लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता।
लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ
| लोकोक्तियाँ | अर्थ |
|---|---|
| अंधा क्या चाहे दो आंखें | बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना |
| नौ दो ग्यारह होना | रफूचक्कर होना या भाग जाना |
| असमंजस में पड़ना | दुविधा में पड़ना |
| आँखों का तारा बनना | अधिक प्रिय बनना |
| आसमान को छूना | अधिक प्रगति कर लेना |
| किस्मत का मारा होना | भाग्यहीन होना |
| गर्व से सीना फूल जाना | अभिमान होना |
| गले लगाना | स्नेह दिखाना |
| चैन की साँस लेना | निश्चिन्त हो जाना |
| जबान घिस जाना | कहते कहते थक जाना |
| टस से मस न होना | निश्चय पर अटल रहना |
| तहस नहस हो जाना | बर्बाद हो जाना |
| ताज्जुब होना | आश्चर्य होना |
| दिल बहलाना | मनोरंजन करना |
| अंधों में काना राजा | मूर्खों में कुछ पढ़ा-लिखा व्यक्ति |
| अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता | अकेला आदमी लाचार होता है। |
| अधजल गगरी छलकत जाय | डींग हाँकना |
| आँख का अँधा नाम नयनसुख | गुण के विरुद्ध नाम होना |
| आँख के अंधे गाँठ के पूरे | मुर्ख परन्तु धनवान |
| आग लागंते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ | नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है। |
| आगे नाथ न पीछे पगही | किसी तरह की जिम्मेदारी न होना |
| आम के आम गुठलियों के दाम | अधिक लाभ |
| ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे | काम करने पर उतारू |
| ऊँची दुकान फीका पकवान | केवल बाह्य प्रदर्शन |
| एक पंथ दो काज | एक काम से दूसरा काम हो जाना |
| कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली | उच्च और साधारण की तुलना कैसी |
| घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध | निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाटा है, पर दूर का ज्यादा |
| चिराग तले अँधेरा | अपनी बुराई नहीं दिखती |
| जिन ढूंढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ | परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। |
| नाच न जाने आँगन टेढ़ा | काम न जानना और बहाने बनाना |
| न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी | न कारण होगा, न कार्य होगा |
| होनहार बिरवान के होत चीकने पात | होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। |
| जंगल में मोर नाचा किसने देखा | गुण की कदर गुणवानों बीच ही होती है। |
| कोयल होय न उजली, सौ मन साबुन लाई | कितना भी प्रयत्न किया जाये स्वभाव नहीं बदलता |
| चील के घोसले में माँस कहाँ | जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। |
| चोर लाठी दो जने और हम बाप पूत अकेले | ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं। |
| चंदन की चुटकी भरी, गाड़ी भरा न काठ | अच्छी वास्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है, जब्कि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती |
| छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच | दिखावटी ठाट-वाट परन्तु वास्तविकता में कुछ भी नहीं |
| छछूंदर के सर पर चमेली का तेल | अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना |
| जिसके हाथ डोई, उसका सब कोई | धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। |
| योगी था सो उठ गया आसन रहा भभूत | पुराण गौरव समाप्त |
| आप भला तो जग भला | अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। |
| जिसकी लाठी उसकी भैंस | बलवान की ही विजय होती है। |
| जैसी करनी वैसी भरनी | किए का फल भोगना पड़ता है। |
| जैसा देश वैसा भेष | जहाँ रहो, वहाँ के रीति-रिवाजों के अनुसार रहो |
| जो गरजते हैं वे बरसते नहीं | अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं। |
| डूबते को तिनके का सहारा | विपत्ति में थोड़ी-सी सहायता भी किसी को उबार सकती है। |
| तेते पाँव पसारिए जेती लाँबी सौर | शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। |
| थोथा चना बाजे घना | ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। |
| दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया | रुपया ही सब कुछ है। |
| दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम | अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होना। |
| दूध का जला छाछ को भी फुँक-फुँक कर पीता है | एक बार धोखा खाकर व्यक्ति सावधान हो जाता है। |
| दूर के ढोल सुहावने | परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना |
| धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का | अस्थिरता के कारण कहीं का न हो पाना |
| न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी | विवाद को जड़ से नष्ट कर देना |
| न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी | शर्त पूरी न होने पर काम का न बनना |
| नाच न जाने आँगन टेढ़ा | स्वयं अयोग्य होना, दोष दूसरों को देना |
| नौ नकद न तेरह उधार | नकद लेन-देन हमेशा अच्छा होता है। |
| पर उपदेश कुशल बहुतेरे | दूसरों को उपदेश देने वाले किंतु स्वयं उस पर आचरण न करने वाले बहुत होते हैं। |
| बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद | मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर करना नहीं जानता |
| बिन माँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख | माँगने से कुछ नहीं मिलता |
| बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय | गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है। |
| भागते भूत की लंगोटी सही | जो मिल जाए वह काफी है। |
| मन चंगा तो कठौती में गंगा | मन शुद्ध है तो सब ठीक है। |
| मुँह में राम बगल में छुरी | ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता |
| मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त | जिसका काम हो, वह सुस्त, उसका समर्थक अधिक सक्रिय |
| रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई | सब बर्बाद हो गया, किंतु शेखी अब भी वही |
| लकड़ी के बल पर बंदर नाचे | डंडे से सब भयभीत होते हैं। |
| लातों के भूत बातों से नहीं मानते | दुष्ट व्यक्ति दंड से ही भयभीत होते हैं। |
| सहज पके सो मीठा होय | धीरे-धीरे सहज रूप से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। |
| साँप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे | काम भी बन जाए और हानि भी न हो |
| साँच को आँच नहीं | सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं |
| सिर दिया ओखल में तो मूसल से क्या डर | जब कोई काम आरंभ किया तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए |
| सीधी उँगली से घी नहीं निकलता | बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं चलता |
| सेवा करे सो मेवा पावै | सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। |
| हाथ कंगन को आरसी क्या | प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं |
| हाथी निकल गया, दुम रह गई | थोड़ा-सा काम अटक जाना |
| हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और | कहना कुछ और करना कुछ |
| हाथी के पाँव में सबका पाँव | एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे-छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। |
| होनहार बिरवान के होत चिकने पात | होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। |
जरूर पढ़िए:-
लोकोक्तियाँ और मुहावरों में अंतर
| मुहावरे | लोकोक्तियाँ |
|---|---|
| मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। जैसे:- अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना आदि। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता हैं तब ये संरचनागत पूर्णता प्राप्त करती है। | लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। इनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। भाषा में प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती है। जैसे:- चार दिन की चाँदनी फेर अँधेरी रात। |
| मुहावरे में लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। | लोकोक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। |
| मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। | लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। |
| मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। | लोकोक्तियाँ वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। |
| वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण परिवर्तन होता है। जैसे:- आँखें पथरा जाना। | लोकोक्तियों में प्रयोग के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे:- अधजल गगरी छलकत जाए। |
| मुहावरों का अंत प्रायः इनफीनीटिव ‘ना’ युक्त क्रियाओं के साथ होता है। जैसे:- हवा हो जाना, होश उड़ जाना, सिर पर चढ़ना, हाथ फैलाना आदि। | लोकोक्तियों के लिए यह शर्त जरूरी नहीं है। चूँकि लोकोक्तियाँ स्वतः पूर्ण वाक्य हैं अतः उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है। जैसे:- अधजल गगरी छलकत जाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, आ बैल मुझे मार, इस हाथ दे, उस हाथ ले, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। |
| मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। जैसे:- हाथ मलना, मुँह फुलाना? | लोकोक्तियाँ जीवन के भोगे हुए यथार्थ को व्यंजित करती हैं। जैसे:- न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती, नाच न जाने आँगन टेढ़ा। |
| मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। | लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। |
| मुहावरों से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ होता है जो लक्षणा शक्ति से निकलता है। | लोकोक्तियों के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होते हैं। |
| मुहावरे ‘तर्क’ पर आधारित नहीं होते अतः उनके वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे:- ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना, छाती पर मूँग दलना। | लोकोक्तियाँ प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियाँ होती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ तर्कशून्य भी हो सकती हैं जैसे : तर्कपूर्ण:- (i). काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती। (ii). एक हाथ से ताली नहीं बजती। (iii). आम के आम गुठलियों के दाम। तर्कशून्य:- (i). छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। |
| मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते। | लोकोक्तियाँ अतिशयोक्तियाँ बन जाती हैं। |
लोकोक्तियों के उदाहरण
1. अधजल गगरी छलकत जाए
अर्थ :- थोड़ी जानकारी वाला बढ़ चढ़कर बोलता है।
वाक्य प्रयोग :- भुवन ने थोड़ा बहुत पढ़ना क्या जान लिया कि अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखो से टकरा जाता है। सच ही कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए।
2. घर की मुर्गी दाल बराबर
अर्थ :- अपने पास की चीज का महत्व नहीं होता
वाक्य प्रयोग :- संजय के पिता एक अच्छे कवि है पर वह अपनी कविताओं को पुष्कर के पास दिखलाने जाता है। ठीक ही कहा गया है घर की मुर्गी दाल बराबर।
3. ऊंची दुकान फीके पकवान
अर्थ :- सिर्फ बाहरी दिखावा
वाक्य प्रयोग :- बार-बार इस विद्यालय का विज्ञापन पढ़कर मैंने अपने बेटे का नामांकन इस विद्यालय में करवाया। आज साल भर हो गए पर उतना का उतना ही जानता है। मैं तो ऊंची दुकान फीके पकवान में पड़ गया।
4. चोर चोर मौसेरे भाई
अर्थ :- बुरे आदमियों का परस्पर संबंध हो जाता है।
वाक्य प्रयोग :- विजय तुमने तो यह देखा कि वह नेता आकर क्या-क्या बोल गया, पर इनकी बातों में हमें नहीं आना है। यह दूसरा थोड़े निकलेगा। सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं।
5. डूबते को तिनके का सहारा
अर्थ :- असहाय को तनिक भी सहारा काफी होता है।
वाक्य प्रयोग :- भैया मैं तुम्हारा लाख-लाख शुक्र गुजार रहूंगा। इस स्थिति में तुमने पैसों की मदद करके डूबते को तिनके का सहारा बनने का काम किया है।
6. आगे नाथ न पीछे पगहा
अर्थ :- बिना जिम्मेवारी का होना।
वाक्य प्रयोग :- रहीम को क्या है आगे नाथ न पीछे पगहा। खा-पीकर इधर-उधर डींगे मारता-फिरता है।
7. खोदा पहाड़ निकली चुहिया
अर्थ :- परिश्रम बहुत करना, लाभ कम पाना
वाक्य प्रयोग :- ओह! मन कचोट कर रह गया। दो बीघे में फसल लगाई थी। आज उसमें से मात्र दो मन अनाज निकला। मैं बदकिस्मत ही तो था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
8. एक पंथ दो काज
अर्थ :- एक बार में दो काम होना
वाक्य प्रयोग :- आज राम पुस्तकालय में बैठा पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक सामने श्याम दिखाई पड़ा। उसने राम को रुपए देते कहा कि तुमने जो उधार पैसे मांगे थे वह हैं। राम के वहां एक पंथ दो काज हो गए।
9. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता
अर्थ :- अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता
वाक्य प्रयोग :- देखो घनश्याम मैं तुम्हें बार-बार कह रहा हूं कि तुम इस काम में औरों की मदद ले लो। सुना नहीं है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
10. आंख का अंधा गांठ का पूरा
अर्थ :- मूर्ख धनवान होना
वाक्य प्रयोग :- उन अफसरों की बात क्या करते हो, घुस के पैसे हैं। वह तो आंख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं।
11. जिसकी लाठी उसकी भैंस
अर्थ :- बलवानों का बोलबाला
वाक्य प्रयोग :- तुम आश्चर्य में क्यों पड़ गए हो अजय। आज यह बात कोई नई नहीं हुई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यह तो शुरु से ही देखने को मिल रहा है।
12. अंत भला तो सब भला
अर्थ :- जिसका परिणाम अच्छा होता है वह सबसे अच्छा होता है।
वाक्य प्रयोग :- रोहन पढ़ने में कमजोर था लेकिन परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला।
13. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत
अर्थ :- समय निकलने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता।
वाक्य प्रयोग :- साल भर मुस्कान ने किताबे खोलकर नहीं देखी और परीक्षा के समय चिंतित हो रही है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
1. अंगूर खट्टे हैं
अर्थ :- वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना।
2. अंडा सिखावे बच्चा को चीं-चीं मत कर
अर्थ :- छोटों द्वारा बड़े को उपदेश देना।
3. अंडे सेवे कोई, लाभ लेवे कोई
अर्थ :- परिश्रम कोई और करें और लाभ किसी दूसरे को मिले
4. अंधा क्या जाने बसंत बहार
अर्थ :- जो वस्तु देखी नहीं, उसका आनंद क्या पता
5. अंधे की लाठी
अर्थ :- बेसहारे को सहारा
6. अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है।
अर्थ :- किसी के सामने उसकी बुराई करने से बुरा ही लगता है।
7. अंधों में काना राजा
अर्थ :- मूर्खों में कम जानने वाले लोगों की प्रतिष्ठा होती है।
8. अकल बड़ी या भैंस
अर्थ :- शारीरिक शक्ति से बड़ी बौद्धिक शक्ति होती है।
9. अपना मकान कोट समान
अर्थ :- अपना घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है।
10. अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग
अर्थ :- अलग-अलग विचार होना।
11. अपनी गली में कुत्ता शेर
अर्थ :- अपने घर में आदमी बलवान होता है।
12. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना
अर्थ :- अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करना।
13. आ बैल मुझे मार
अर्थ :- जानबूझकर मुसीबत मोल लेना।
14. आग कह देने से मुंह नहीं जल जाता।
अर्थ :- किसी को कोसने से उसका बुरा नहीं हो जाता।
15. आग खाएगा तो अंगार ही उगलेगा
अर्थ :- बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।
16. आग बिना धुआं नहीं
अर्थ :- बिना कारण कुछ नहीं होता।
17. आगे कुआं पीछे खाई
अर्थ :- सभी ओर से मुसीबत आना।
18. आदमी का दवा आदमी है।
अर्थ :- मनुष्य की सहायता मनुष्य ही करता है।
19. आप भला तो जग भला
अर्थ :- अच्छे आदमी को पूरा संसार अच्छा ही लगता है।
20. आम के आम गुठलियों के दाम
अर्थ :- दोगुना लाभ
21. आसमान का थुका मुंह पर आता है।
अर्थ :- बड़े लोगों की बुराई करने से अपनी ही बुराई होती है।
22. आसमान से गिरा खजूर पर अटका
अर्थ :- सफलता में कई बाधाएं आना।
23. ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया
अर्थ :- संसार में कहीं सुख है तो कहीं दुख है।
24. उतावला सो बावला
अर्थ :- मूर्ख व्यक्ति जल्दीबाजी में काम करते हैं।
25. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
अर्थ :- अपनी गलती किसी और पर थोपना।
26. एक अनार सौ बीमार
अर्थ :- एक ही वस्तु को कई लोग द्वारा पाने की कोशिश करना।
27. एक ही थाली के चट्टे बट्टे
अर्थ :- एक ही समान व्यवहार वाला होना।
28. एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा करती है।
अर्थ :- एक बुरा व्यक्ति अपने आसपास के सभी व्यक्ति को बुरा बना देता है।
29. एक हाथ से ताली नहीं बजती
अर्थ :- झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है।
30. कंगाली में आटा गीला
अर्थ :- मुसीबत में और मुसीबत आना
31. कब्र में पाव लटकना
अर्थ :- अधिक उम्र का होना।
32. कभी के दिन बड़े, कभी की रात
अर्थ :- सभी दिन एक समान नहीं होते हैं।
33. कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर
अर्थ :- परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
34. कर सेवा तो खा मेवा
अर्थ :- अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है।
35. करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान
अर्थ :- अभ्यास करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है।
36. कल किसने देखा है
अर्थ :- आज का काम आज ही करना चाहिए।
37. कागज की नाव नहीं चलती
अर्थ :- बेईमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलती।
38. कान में तेल डालकर बैठना
अर्थ :- सभी चिंता छोड़ कर बैठना।
39. काबुल में क्या गधे नहीं होते
अर्थ :- अच्छाई के साथ-साथ बुराई भी होती है।
40. काम को काम सिखाता है
अर्थ :- काम करने से आदमी होशियार हो जाता है।
41. काला अक्षर भैंस बराबर
अर्थ :- अनपढ़ होना
42. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है
अर्थ :- देखा देखी काम करना।
43. खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे
अर्थ :- अपनी असफलता पर खीझना
44. खुदा गंजे को नाखून नहीं देता
अर्थ :- ईश्वर सबकी भलाई का ध्यान रखता है।
45. ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता
अर्थ :- केवल सोचने से काम नहीं होता।
46. गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता
अर्थ :- स्वभाव नहीं बदलता
47. गरीब की लुगाई सबकी भौजाई
अर्थ :- गरीब व्यक्ति का सब लाभ उठाते हैं।
48. गर्व का सिर नीचा
अर्थ :- घमंडी आदमी का घमंड चूर-चूर हो ही जाता है।
49. गागर में सागर भरना
अर्थ :- कम शब्द में अधिक बात कहना।
50. गुड़ खाए गुलगुले से परहेज
अर्थ :- ढोंग करना
51. गेहूं के साथ घुन भी पिसता है
अर्थ :- दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी मर जाता है।
52. घर का भेदी लंका ढाए
अर्थ :- आपसी फूट के कारण भेद खोलना।
53. घी गिरी लेकिन खिचड़ी में
अर्थ :- गलती से भी अच्छा काम हो जाना।
54. घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या
अर्थ :- व्यापार में रियायत नहीं की जाती।
55. चट मंगनी पट ब्याह
अर्थ :- अच्छा काम जल्दी ही कर देना चाहिए।
56. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए
अर्थ :- बहुत कंजूस होना
57. चलती का नाम गाड़ी
अर्थ :- काम होते रहना चाहिए।
58. चांद को भी ग्रहण लगता है।
अर्थ :- भले आदमी की भी बदनामी होती है।
59. चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात
अर्थ :- सुख थोड़े ही दिन का होता है।
60. चिराग तले अंधेरा
अर्थ :- अपना दोष स्वयं न दिखाई देना
जरूर पढ़िए :
उम्मीद है लोकोक्तियाँ की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।
लोकोक्तियाँ से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करे।
यदि लोकोक्तियाँ की यह जानकारी पसंद आयी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे और सोशल मीडिया पर शेयर करें।